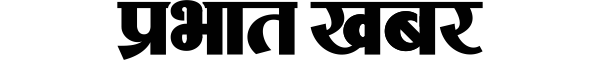एक विफल व्यवस्था के नतीजे
घनश्याम शाह सोशल साइंटिस्ट editor@thebillionpress.org अपने-अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था तथा हुकूमत में प्रभावशाली कृषक जातियां शिक्षण संस्थानों तथा नौकरियों में आरक्षण हेतु अपने संघर्ष से विमुख होती नहीं लगतीं. महाराष्ट्र में मराठा, तो गुजरात में पाटीदार, हरियाणा-राजस्थान में जाट, तो आंध्र और तेलंगाना में कापू समुदाय के साथ यही स्थिति जारी है. इस वर्ष की […]
घनश्याम शाह
सोशल साइंटिस्ट
editor@thebillionpress.org
अपने-अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था तथा हुकूमत में प्रभावशाली कृषक जातियां शिक्षण संस्थानों तथा नौकरियों में आरक्षण हेतु अपने संघर्ष से विमुख होती नहीं लगतीं. महाराष्ट्र में मराठा, तो गुजरात में पाटीदार, हरियाणा-राजस्थान में जाट, तो आंध्र और तेलंगाना में कापू समुदाय के साथ यही स्थिति जारी है.
इस वर्ष की शुरुआत में गुजरात की एक घटना मीडिया तथा जनमानस का ध्यान आकृष्ट करने में विफल रही, जिसके अंतर्गत वहां के पाटीदार कारोबारियों ने तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफाॅर्म की स्थापना का फैसला किया, जिसके द्वारा एक लाख पाटीदार युवाओं को रोजगार मुहैया किया जायेगा.
जहां मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने इस सम्मेलन में उपस्थित होकर इस मुहिम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया, वहीं प्रबुद्ध वर्ग के कई लोगों ने भी इसकी तारीफ करते हुए दूसरे समुदायों से इसका अनुकरण करने की अपील की. कठिनाई यह है कि अधिकतर निचली जातियों में इस हेतु न तो पर्याप्त संख्या में धनवान उद्यमी हैं और न ही उनके पास उतनी सामाजिक पूंजी है.
हमारी सियासी प्रणाली इस तरह की जातिगत एकजुटता के पोषण हेतु अनुकूल मंच मुहैया करती है. यदि अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन में किसी प्रभावशाली जाति का दबदबा हो, तो उस जाति के गरीब तबके से आनेवाले लोग कई तरह के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ की स्थिति में होते हैं.
औपनिवेशिक तथा उपनिवेश पश्चात के राज्यों ने प्रभावशाली जातियों को वित्तीय तथा सामाजिक-सांस्कृतिक पूंजी इकठ्ठा करने की सहूलियतें प्रदान कीं. इन जातियों के संघों तथा मंचों ने अपनी जातियों के सदस्यों के लिए कई तरह के कल्याणकारी कदमों के अलावा उनके लिए स्कूल-कॉलेज, कोचिंग तथा छात्रवृत्तियां शुरू कीं. सफल उद्यमियों की बहुलतावाली जातियों ने अपनी बिरादरी के लोगों द्वारा कोई उद्यम आरंभ करने के लिए ऋण उपलब्ध करने की प्रणाली विकसित की. वे अपनी फर्मों की भर्तियों में भी अपनी जाति के लोगों को वरीयता देते हैं.
इन सभी लाभप्रद स्थितियों के बावजूद इन प्रभावशाली जातियों के शिक्षित युवा आरक्षण की मांग उठा रहे हैं, जो पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण समाप्त करने की उनकी प्रारंभिक मांग से बहुत भिन्न है.
विकास के हमारे मॉडल के अंतर्गत इन प्रभावशाली जातियों ने राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों तथा हरित क्रांति के बूते अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत तो कर ली, पर हमारे यहां कारोबारी स्थितियां कृषि से अधिक उद्योगों की पक्षपाती रहीं. गुजरात के विपरीत, महाराष्ट्र में कुछ पिछड़ी जातियों ने अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर ली और कृषि के क्षेत्र में भी वे मराठा समुदाय से स्पर्धा कर रही हैं.
कुल मिलाकर, पिछले अरसे में कृषकों का अनुपात कम हुआ है. लोकनीति-सीएसडीएस द्वारा वर्ष 2013-14 में किये एक सर्वेक्षण के अनुसार, 65 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक तथा 50 प्रतिशत मध्यम किसान कृषि को छोड़कर शहरों में बसना चाहते हैं.
सबकी तरह, मराठा तथा पाटीदार भी औपचारिक शिक्षा को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एकमात्र संपदा समझते हैं, ताकि वे अच्छी और सुरक्षित नौकरियां पा सकें. उच्च शिक्षा में पिछड़ी जातियां तेजी से उनकी बराबरी में पहुंच रही हैं. यह उनके अहं पर चोट करते हुए उन्हें भयभीत करता है कि वे उनसे आगे भी निकल जा सकते हैं.
उनमें से अधिकतर सामान्य शिक्षा हासिल करने के लिए सरकारी एवं सामान्य निजी कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, जो उपकरणों एवं स्टाफ की कमी से पीड़ित होने के अलावा पुराने पाठ्यक्रमों की शिक्षा देते हैं.
यह शिक्षा अब उन्हें पर्याप्त और नियोक्ताओं की जरूरत के हिसाब से कौशल नहीं देती है. विदेशों का रुख करनेवाले पाटीदारों को वहां अपने कौशल के अवमूल्यन का सामना कर शून्य से शुरुआत करनी पड़ी. इसने भी उन्हें हताश किया. उनमें से बहुतों के पास अपने उद्यम आरंभ करने योग्य चतुराई, कौशल, अनुभव एवं पूंजी का अभाव है. शहरी रोजगारियों का 80 प्रतिशत से भी अधिक 20 हजार रुपये प्रतिमाह से कम ही अर्जित कर पाता है. ऐसी स्थिति में वे पाते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प वेतनयुक्त नियमित नौकरी ही है.
रोजगार का सर्वाधिक विकास अनौपचारिक क्षेत्र में ही हुआ है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा की सुविधा नहीं है. औपचारिक क्षेत्र में भी उपलब्ध रोजगार प्रायः आकस्मिक तथा संविदा आधारित हैं. ऐसे जॉब उनकी बढ़ती जरूरतें, जीवनशैली तथा सामाजिक स्थिति की अवधारणा तुष्ट नहीं कर सकते. ऐसे में एक शिक्षित युवा महसूस करता है कि सरकारी नौकरी ही सुरक्षा तथा गरिमामय स्थिति प्रदान करती है.
प्रभावशाली जातियों के क्रुद्ध युवा इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते कि निचली जातियां ऊपर उठकर अपनी जीवनशैली उन्नत कर चुकी हैं. इसके साथ ही, वे इससे भी हताश हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था उनकी आकांक्षाएं और आवश्यकताएं तो बढ़ा देती है, पर उन्हें एक अच्छा रोजगार नहीं दे सकती. यह उन्हें अपनी शुरुआती पहचान पर निर्भरता हेतु बाध्य कर देती है और हमारी सियासी व्यवस्था भी संस्कृति के नाम पर उनकी इसी पहचान को परिपुष्ट करती है. यही इन सारी परिस्थितियों की विडंबना है.
(अनुवाद: विजय नंदन)